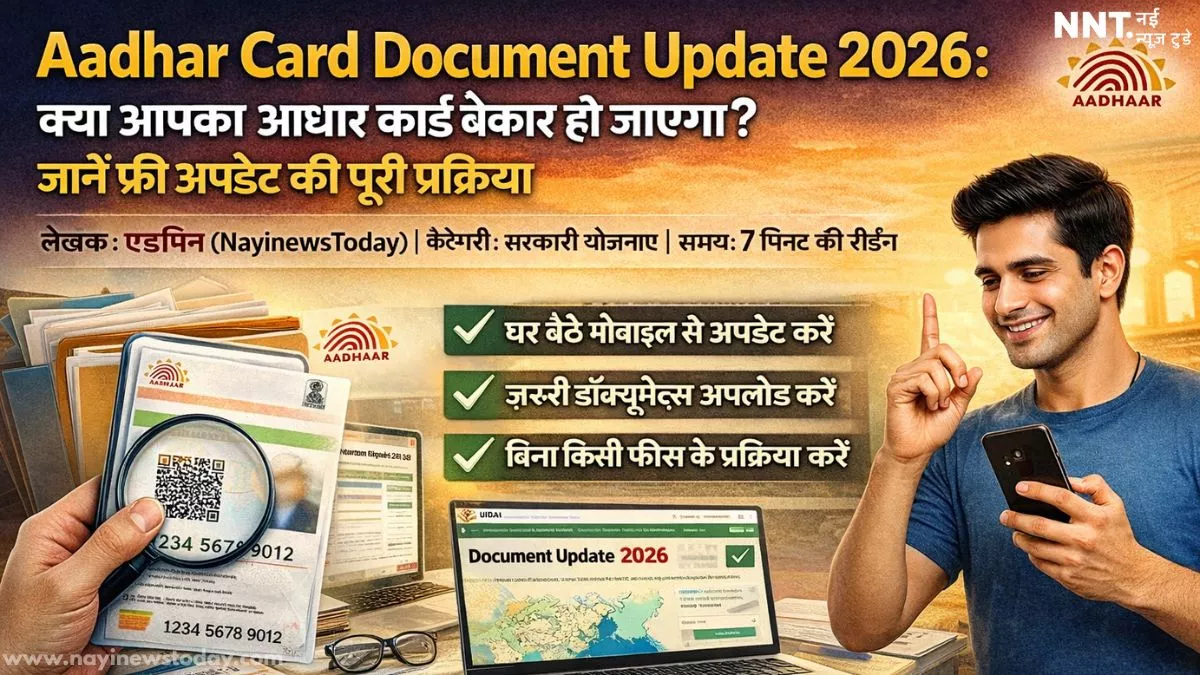सुप्रीम कोर्ट का Big Order: दिल्ली में लावारिस कुत्तों पर सख्त कार्रवाई, बाधा डालने वालों पर होगा Action
दिल्ली में लावारिस कुत्तों (stray dogs) की बढ़ती संख्या और रेबीज (rabies) के मामलों को लेकर चिंता लंबे समय से जताई जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को निर्धारित समयसीमा में व्यवस्थित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का केंद्र बिंदु यह है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे कुत्तों को नियमानुसार पकड़कर डॉग शेल्टर में स्थानांतरित किया जाए, उनका बधियाकरण (ABC – Animal Birth Control) और टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए, तथा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यवस्थाएं पुख्ता की जाएं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
पूरा मामला क्या है?
राजधानी में आवारा कुत्तों से जुड़े घटनाक्रम—काटने की शिकायतें, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की चिंता, रिहायशी इलाकों में झुंडों की मौजूदगी—लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। अलग-अलग नागरिक समूहों, RWAs और अभिभावक संगठनों की ओर से याचिकाएं और पत्राचार होते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पशु-कल्याण से जुड़े कार्यकर्ता यह मांग उठाते रहे हैं कि समाधान मानवीय और कानूनी प्रोटोकॉल (ABC Rules, Vaccination) के अनुरूप हो। ऐसे परस्पर विरोधी दबावों के बीच अदालत का यह आदेश व्यवस्था, जवाबदेही और समयसीमा तय करता है।
यह आदेश कब और क्यों आया?
दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर असर डालने वाले मुद्दों—जैसे रेबीज के संभावित जोखिम—को देखते हुए अदालत ने प्रशासन से एक ठोस एक्शन प्लान चाहा। अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में यह चिंता प्रमुख थी कि अनियंत्रित प्रजनन और समय पर टीकाकरण न होने से संकट बढ़ता है। साथ ही, शेल्टरों की सीमित क्षमता और मैदान-स्तर पर समन्वय की कमी भी चुनौती रही है। न्यायालय ने व्यवस्था में सुधार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए, ताकि मानवीय दृष्टिकोण बरकरार रखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सार
पहला—निश्चित समयसीमा में आवारा कुत्तों को पकड़कर सरकारी/मान्यता प्राप्त डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए।
दूसरा—बधियाकरण (Animal Birth Control) और रेबीज वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाए ताकि अनियंत्रित प्रजनन रुके और संक्रमण का जोखिम घटे।
तीसरा—निरीक्षण और पारदर्शिता के लिए शेल्टर्स में CCTV निगरानी तथा रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित हो।
चौथा—जो लोग/संस्थान पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आवश्यक होने पर अदालत-अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है।
पांचवां—नवजात और छोटे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए; संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त और त्वरित रिस्पॉन्स की व्यवस्था हो।
दिल्ली में आवारा कुत्तों की चुनौती: जमीनी तस्वीर
राजधानी के कई इलाकों में फीडिंग प्वाइंट और बस्तियों के पास कुत्तों के झुंड देखे जाते हैं। रात के समय सड़कों, पार्कों और कॉलोनियों के भीतर इनकी गतिविधि बढ़ जाती है। कुछ जगहों पर काटने के मामलों और स्कूलों के बाहर बच्चों के साथ झुंड का पीछा करने की खबरें चिंता बढ़ाती रही हैं। इन घटनाओं के कारण माता-पिता, स्कूल प्रबंधन और स्थानीय निवासी सुरक्षा-उन्मुख कदमों की मांग करते रहे हैं।
उधर, पशु-कल्याण समूह कहते हैं कि जहां-जहां ABC और टीकाकरण व्यवस्थित रूप से हुआ, वहां काटने के मामले और आक्रामक व्यवहार में कमी देखी गई। अतः समाधान का टिकाऊ रास्ता “पकड़ो–बधियाकरण–टीकाकरण–रिहैब/रीहोमिंग” के फ्रेमवर्क में ही निहित है। अदालत का आदेश इसी दिशा में स्पष्ट, मापने योग्य और जवाबदेही-आधारित रोडमैप तय करता है।
शेल्टर क्षमता, स्टाफ और संसाधन: असली कसौटी
इस आदेश का सबसे बड़ा व्यावहारिक पक्ष है—पर्याप्त शेल्टर क्षमता, प्रशिक्षित स्टाफ, चिकित्सा सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स। शेल्टरों में मानवीय देखभाल—साफ-सफाई, भोजन-पानी, नियमित स्वास्थ्य जांच, आइसोलेशन वार्ड—और रिकॉर्ड-मैनेजमेंट आवश्यक है। यदि बड़े पैमाने पर कुत्तों को लाया जाना है, तो एक्सपर्ट वेटरनरी टीम, एम्बुलेंस/मोबाइल यूनिट्स, ऑन-साइट ऑपरेशन थिएटर और रिकवरी केयर की ठोस व्यवस्था चाहिए।
अदालत ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CCTV निगरानी और डेटा-डैशबोर्ड जैसी बातों पर जोर दिया है। इससे नागरिक समाज और न्यायालय के समक्ष प्रगति का ऑडिट संभव होगा—कितने कुत्ते पकड़े/बधियाकृत हुए, वैक्सीनेशन कवरेज कितना बढ़ा, रिकवरी/रीहोमिंग का अनुपात क्या है, इत्यादि।
कानूनी और सामाजिक संतुलन: अधिकार बनाम सुरक्षा
दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर दो चरम विचार मौजूद रहे हैं—एक ओर सार्वजनिक सुरक्षा और बच्चों की रक्षा का सवाल है, दूसरी ओर पशु-कल्याण और दया का मूल मूल्य। अदालत के आदेश का महत्व इस बात में है कि कानून-सम्मत और मानवीय प्रक्रिया के भीतर व्यवस्थित समाधान निकाला जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया में बाधा बनना स्वीकार्य नहीं होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पशु-कल्याण कार्यकर्ताओं की भूमिका खत्म हो गई; बल्कि उनसे अपेक्षा है कि वे निर्धारित नियमों—जैसे ABC, टीकाकरण, शेल्टर प्रोटोकॉल—के साथ सहयोग करें। यही सहयोग मॉडल दीर्घकालिक समाधान देता है।
बच्चों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा पर फोकस
आदेश में नवजात और छोटे बच्चों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। स्कूल-ज़ोन्स, पार्क, एंगनवाड़ी, डिस्पेंसरी के आसपास हॉट-स्पॉट सर्वे कर तेज़ कार्रवाई की जरूरत होगी। जन-जागरूकता भी उतनी ही अहम है—बच्चों को सिखाया जाए कि कुत्तों के साथ कैसे व्यवहार करें, उन्हें उकसाने वाले व्यवहार से कैसे बचें, और काटने की स्थिति में First Aid व Anti-Rabies Protocol क्या है।
प्रशासन की चुनौती: समयसीमा और क्रियान्वयन
न्यायालय ने एक स्पष्ट समयरेखा दी है, जिसका पालन स्थानीय निकाय, नगर निगम, पशु चिकित्सालय और संबंधित विभागों के समन्वय से ही संभव है। माइक्रो-प्रोजेक्ट प्लान—वार्ड-वाइज टीम, दैनिक लक्ष्य, सप्ताहिक रिव्यू, तथा पब्लिक हेल्पलाइन—से फील्ड-इम्प्लीमेंटेशन मजबूत होगा।
साथ ही, डेटा-आधारित निर्णय लेने की संस्कृति जरूरी है: किन वार्डों में अधिक शिकायतें हैं, कहाँ वैक्सीनेशन गैप बड़ा है, किन शेल्टर्स में ओवरक्राउडिंग का खतरा है, कहाँ रीहोमिंग/एडॉप्शन के अवसर हैं—इन सब पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
नागरिकों की भूमिका: शिकायत से सहयोग तक
यह मुद्दा केवल प्रशासन का नहीं है। नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है—समय पर शिकायत दर्ज कराना, फीडिंग को चिह्नित पॉइंट पर और प्रोटोकॉल के साथ करना, कूड़े-कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण ताकि फूड-एट्रैक्शन कम हो, और शेल्टर/ABC ड्राइव के दौरान मैदानी टीमों के साथ सहयोग करना।
जो नागरिक या समूह दया-भाव से फीडिंग करते हैं, वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेजिस्ट्रेशन, फिक्स्ड टाइम–फिक्स्ड स्पॉट और पोस्ट-फीड क्लीनअप जैसे नियम अपनाएं। इससे विवाद कम होंगे और मानवीय समाधान के साथ सार्वजनिक सुरक्षा भी बनी रहेगी।
लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी: “पकड़ो नहीं, नियंत्रित करो”
वैश्विक अनुभव बताते हैं कि सिर्फ हटाने से समस्या जड़ से खत्म नहीं होती; खाली जगहों पर दूसरे कुत्ते आ जाते हैं—इसे “वैकेंसी इफेक्ट” कहते हैं। टिकाऊ समाधान ABC + टीकाकरण + फीडिंग-नियम + कचरा-प्रबंधन + शेल्टर-अपग्रेड + एडॉप्शन के कंबाइंड मॉडल में है। सुप्रीम कोर्ट का Big Order इसी समेकित दृष्टिकोण को लागू करने की दिशा में बाध्यकारी ढांचा देता है।
निष्कर्ष
दिल्ली के लिए यह आदेश एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है—बशर्ते क्रियान्वयन समयबद्ध, डेटा-ड्रिवेन और मानवीय हो। सड़क सुरक्षा और पशु-कल्याण के बीच संतुलन बनाना ही असली मंथन है। अदालत ने जवाबदेही तय कर दी है; अब बारी है—प्रशासन, नागरिक समाज, पशु-कल्याण समूहों और आम लोगों की—जो मिलकर दिल्ली को सुरक्षित, संवेदनशील और जिम्मेदार शहर बना सकते हैं।
नोट: यह खबर न्यायिक आदेश से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी पर आधारित रिपोर्टिंग है। किसी भी तरह का फेक/बनावटी विवरण शामिल नहीं किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी अस्पताल/हेल्पलाइन और स्थानीय प्रशासन से तुरंत संपर्क करें, तथा आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें।